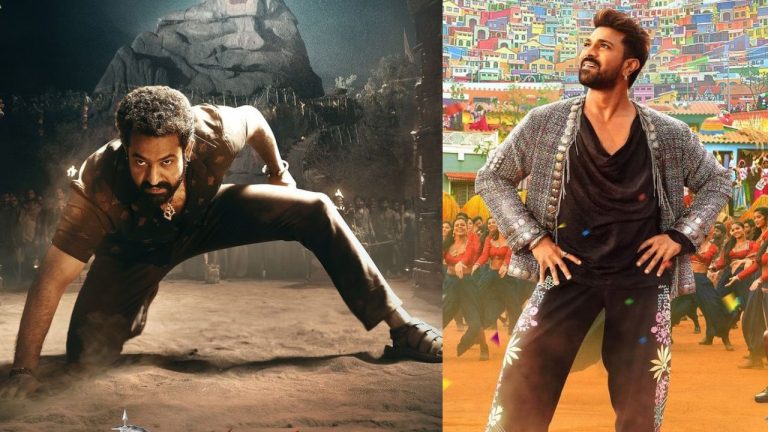Bhakshak Movie Review: सिस्टम के गाल पर तमाचा जड़ती एक सधी हुई जरूरी फिल्म

भक्षक शब्द सुनते ही शक्तिमान याद आ जाता है. उसका एक एपिसोड है, जिसमें लड़का अखबार बेचते हुए एक ही लाइन दोहराता है: रक्षक बना भक्षक, रक्षक बना भक्षक. आज जिस फ़िल्म को देखा गया, उसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है. फ़िल्म का नाम आप हेडलाइन से जान ही गए हैं, बताने की ज़रूरत है नहीं.
भूमि पेडनेकर पत्रकार बनी हैं. वो पटना में कोशिश नाम से अपना एक चैनल एस्टैब्लिश करने की जुगत में हैं. संजय मिश्रा उनके साथ कैमरापर्सन की भूमिका में हैं. आदित्य श्रीवास्तव(CID वाले अभिजीत) विलेन का रोल प्ले कर रहे हैं. पिक्चर नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. मुजफ्फरपुर(बिहार) बालिकागृह कांड से प्रेरित है. वहां के एक शेल्टरहोम में बच्चियों के साथ लगातार रेप हुआ. उन्होंने विरोध किया, चिल्लाई, तो जान से मार दिया गया. फ़िल्म का ओपनिंग सीन ही यही है.
एक भक्षक लड़की के विरोध करने पर उसकी योनि में मिर्च डाल देता है. लड़की दर्द से चिल्लाना शुरू करती है. डॉक्टर को फ़ोन घुमाया जाता है. वो आने में असमर्थता जताता है. लड़की को बड़ी आसानी से मुंह पर तकिया रखकर मार दिया जाता है. जो लोग ये सब कर रहे होते हैं, उनके माथे पर ऐसा करते हुए ज़रा भी शिकन नहीं आती. उनके लिए ये नहाने-धोने, खाने-पीने जैसा रूटीन वर्क है. ओपनिंग सीन असहज ज़रूर करता है, पर बहुत तेज़ी से घटता है. विजुअल और बैकग्राउंड म्यूजिक के ज़रिए सीन अपने क्रेसेंडो तक पहुंचने से पहले ही स्खलित हो जाता है. थ्रिलर फिल्मों में आधा काम उसका बीजीएम करता है. पर यहां उस उच्च कोटि का बैकग्राउंड स्कोर नहीं है. संजय मिश्रा की ही एक फ़िल्म है वध, कुछ वैसा बैकग्राउंड स्कोर इस फ़िल्म की मांग था.
हालांकि हो ये भी सकता है कि डायरेक्टर पुलकित इसे ओवरड्रामेटिक न बनाना चाह रहे हों. ऐसा फ़िल्म में दिखता भी है. फ़िजूल की नाटकीयता दर्शकों और किरदारों पर थोपी नहीं गई है. जैसे वैशाली सिंह(भूमि) का इंट्रोडक्शन हो या बंसी साहू(आदित्य श्रीवास्तव) का, इनमें कोई बहुत ज़्यादा माहौल बनाने का प्रयास नहीं हुआ है. कई लोगों को ये बात नापसंद भी हो सकती है कि भक्षक में ड्रामा बहुत कम है, लेकिन मेरे लिए ये फ़िल्म का प्लस पॉइंट है. ऐसी फिल्मों में अक्सर फ़ास्ट पेस्ड एडिंग रखी जाती है. डायरेक्टर आड़े-तिरछे कैमरा एंगल्स और लो-की लाइटिंग के ज़रिए दर्शकों को बांधकर रखना चाहता है. यहां ठीक इसका उलट है. कहानी में घुलती हुई एडिटिंग, सहज कैमरा शॉट्स और नेचुरल लाइटिंग.
फ़िल्म शेल्टरहोम रेप केस के मुद्दे के पैरलल सोशल-पॉलिटिकल कमेंट्री करती हुई भी चलती है. एक सीन है, जहां पर वैशाली के लेट घर आने तक उसका पति भूखा बैठा रहता है. ऐसे में वैशाली कहती है, “एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी दाल लेकर सीटी मारनी है. बस यही करना है. नहीं कर सकते हो? बच्चे हो क्या? अगर भूख लगी है तो उसे मिटाना भी सीख लो.” ये सीन स्त्रियों के प्रति समाज के सोचने के तरीके की पड़ताल करता है, और उस सोच पर तमाचा भी रसीद करता है.
फ़िल्म में गुप्ता जी का किरदार बहुत दिलचस्प लगा. इसे पंचायत में बनराकस बने दुर्गेश कुमार ने निभाया है. वो अंदर की इन्फॉर्मेशन लाकर वैशाली सिंह को देता है. जब उससे भास्कर(संजय मिश्रा) कहता है, “आपके कहने पर सबका भेद खोल दें और सरकार से दुश्मनी ले लें?” इस पर गुप्ताजी कहते हैं, “तब लिट्टी चोखा बेचिए ना, किराना दुकान खोलिए. पत्रकारिता में काहे घुसे. ये किरदार दिलचस्प है, पर अधूरा है.” इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देनी चाहिए थी. ये एक्जेक्टली क्या करता है? इसका बैकग्राउंड क्या है? खैर वो जो भी हो, दुर्गेश कुमार ने काम जबरदस्त किया है. उनका पंचायत जैसा ही रोल इसमें भी है. बस यहां वो हीरो के पक्ष में हैं.
भास्कर का किरदार बहुत अच्छा लिखा गया है. पर शायद संजय मिश्रा की जगह कोई और होता, तो ये रोल निखरकर नहीं आ पाता. उन्होंने भास्कर को जीवंत कर दिया है. उन्हें देखकर लगता है कि कोई पका हुआ, अनुभवी कैमरापर्सन है. हर तरह के दंदफंद उसको पता हैं. एक सीन है जिसमें संजय मिश्रा एक लड़की से शेल्टरहोम के बारे में कुछ जानकारी जुटा रहे होते हैं. वहां वो जिस तरीके से अपने प्रश्न के बाद, उस लड़की से हुंकारी भराने के लिए आएं कहते हैं, अद्भुत जेस्चर है. संजय हर नई फिल्म में अपनी अदाकारी के नए मानक सेट कर रहे हैं. उन्होंने इस फ़िल्म को अपनी प्रेजेंस से एक अंगुल ऊपर उठा दिया है.
वैशाली के रोल में भूमि पेडणेकर जची हैं. उन्होंने बिहारी एक्सेंट भी ठीक पकड़ा है. कुलमिलाकर उनका काम और स्क्रिप्ट का चुनाव दोनों अच्छा है. जहां अंडरटोन रहना था, वहां उन्होंने बहुत सधा हुआ काम किया है. जिन एकाध जगहों पर उन्हें फट पड़ना था, उन सीन्स में भूमि थोड़ा कमतर साबित हुई हैं. बाक़ी टोटैलिटी में उनकी एक्टिंग सहज और अच्छी है. आदित्य श्रीवास्तव को बहुत दिनों बाद स्क्रीन पर कोई मेजर रोल करते देखकर अच्छा लगता है. उन्होंने बंसी साहू नाम के विलेन को मानवीय बनाए रखा है. लगता है कोई अपने ही बीच का आदमी भक्षक बन गया है. उनके हिस्से भारी-भरकम संवाद नहीं आए हैं, फिर भी वो चमकते हैं.
फ़िल्म छोटे शहर के पत्रकारों के स्ट्रगल और उनके जज़्बे को बड़े साफ-सुथरे ढंग से पेश करती है. ऊपर से जर्निलस्ट के महिला होने और अपने दम पर खुद का चैनल खड़ा करने का संघर्षशील तड़का लगाती है. रिपोर्टिंग की डिटेलिंग पर काम करती है. पुलिस, शासन और प्रशासन की लेयर्ड मिलीभगत की परतें उधेड़ती है. फ़िल्म के कई दृश्य देखकर TSP के शो रबीश की रिपोर्ट का एक किरदार याद आता है. वो कहता है, “सिस्टम रबीश जी सिस्टम”
कुछ फिल्में अच्छी होती हैं, कुछ बुरी. पर कुछ ज़रूरी भी होती हैं. भक्षक उन्हीं में से एक है. देख लीजिए. बाक़ी बंसी साहू के शब्दों को सिर के बल उलट दें, तो एक वाक्य बनता है – इस दुनिया में कोई भी काम हर आदमी के अपने-अपने ढंग से गलत होता है, सही तो कुछ होता ही नहीं. ठीक ऐसे ही फ़िल्म मेरे लिए सही हो सकती है, पर आपके लिए हो सकता है न हो. लेकिन इस निर्णय तक पहुंचने के लिए फ़िल्म कम से कम बार तो देखनी ही पड़ेगी. अलविदा.